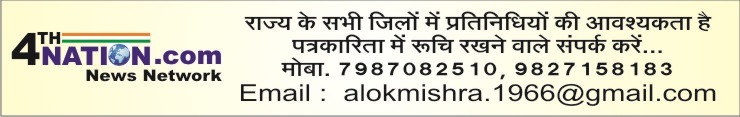छत्तीसगढ़ के बस्तर में हाल के दिनों में आदिवासियों की लगातार हो रही हत्याएं एक गंभीर मानवीय और राजनीतिक संकट बन चुकी हैं। लेकिन इससे भी बड़ा संकट वह है, जो दिल्ली की सत्ता गलियों में पसरा है — गहरी, सुनियोजित और खतरनाक चुप्पी।
जब संसद सत्र चल रहा था, तब बस्तर की घटनाओं पर न कोई बहस हुई, न कोई बयान, न कोई मांग उठी। सत्तारूढ़ दल खुलकर यह कहता है कि वह “नक्सलवाद का सफाया” कर रहा है, और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसे गर्व के साथ दोहराते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्ष—जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है—इस विषय पर पूरी तरह मौन है।
राहुल गांधी, शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, ओवैसी जैसे नेता, जो संविधान और जनतंत्र की रक्षा की बातें करते हैं, इस पर चुप क्यों हैं? क्या यह एक अघोषित सहमति है कि बस्तर की हत्याओं को “राष्ट्रहित” में अनदेखा किया जाए? क्या लोकतंत्र का पूरा ढांचा—संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका—एक साझा भय के तहत संचालित हो रहा है?
इतिहास गवाह है कि सलवा जुडूम, ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऑपरेशन स्टीपलचेज जैसे सैन्य अभियानों को बिना किसी कानूनी घोषणा के अंजाम दिया गया, और आज वही रणनीति नए चेहरे के साथ दोहराई जा रही है। न कोई आदेश पत्र, न कोई सरकारी बयान—सब कुछ “पेपर ट्रेल” से परे, ताकि कोई जवाबदेही तय न हो सके।
यह लोकतंत्र की ‘अधिनायकवादी स्वीकृति’ है—जहां कानून के शासन की बात करने वाले भी अपवाद को “नव-नियम” मानकर चुप्पी साध लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश भी बस्तर में लागू नहीं होते, क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि इस विषय पर उसकी “प्रगतिशील टिप्पणियां” जमीन पर नहीं उतरेंगी।
बस्तर की आदिवासी जनता को जिस तरह से “अंदरूनी दुश्मन” मान लिया गया है, उससे यह साफ होता है कि भारत का लोकतंत्र एक अदृश्य भय पर टिका हुआ है—एक ऐसा भय जो पूरे राजनीतिक तंत्र को जोड़ता है।
यह चुप्पी केवल राजनीतिक विफलता नहीं है, यह उस “संवैधानिक नैतिकता” की विफलता है, जिस पर भारत गर्व करता है। यह वह क्षण है जब लोकतंत्र को अपने ही प्रतिबिंब से डर लगने लगता है।
अब सवाल उठता है — क्या भारतीय लोकतंत्र की आत्मा अब इतनी निर्जीव हो चुकी है कि वह बस्तर जैसे ज्वलंत मुद्दे को भी “संरचनात्मक आवश्यकता” मानकर अनदेखा कर दे?