छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे इलाक़े 2000 के दशक में लगातार माओवादी हिंसा से जूझ रहे थे। इसी दौर में वर्ष 2005 में एक राज्य प्रायोजित अभियान ‘सलवा जुडूम’ की शुरुआत हुई। गोंडी भाषा में सलवा जुडूम का अर्थ है – शांति यात्रा, लेकिन इसकी परिभाषा बस्तर के हजारों आदिवासी परिवारों के जीवन में हिंसा, विस्थापन और पीड़ा बनकर उतर आई।
शुरुआत और मक़सद
सलवा जुडूम का जन्म माओवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हुआ। इसे छत्तीसगढ़ सरकार का खुला समर्थन मिला। बताया जाता है कि खनन समझौतों के बाद राज्य को इन इलाकों से माओवादियों की पकड़ तोड़नी थी। स्थानीय युवाओं और आदिवासियों को इस मुहिम में शामिल किया गया, जिन्हें प्रशिक्षण और संसाधन भी सरकार ने उपलब्ध कराए।
उस समय दावा किया गया कि यह आंदोलन माओवादियों के ख़िलाफ़ एक “जन-जागरण अभियान” है। गाँव-गाँव रैलियाँ निकाली गईं और लोगों को “माओवादी समर्थकों” और “सरकारी समर्थकों” में बाँट दिया गया।
गतिविधियाँ और विवाद
समय के साथ यह आंदोलन विवादों में घिरता चला गया। सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं और अर्धसैनिक बलों पर कई गंभीर आरोप लगे।
- गाँवों को जबरन खाली कराया गया और लोगों को सरकारी कैंपों में रहने को मजबूर किया गया।
- नाबालिगों की भर्ती की गई और उन्हें हथियार उठाने को कहा गया।
- जिन गाँवों ने साथ नहीं दिया, उन्हें “माओवादी” घोषित कर दिया गया और वहाँ मूलभूत सुविधाएँ रोक दी गईं।
- कई गाँवों को जलाने, लूटने और ग्रामीणों की हत्याओं तक के आरोप लगे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और कई मानवाधिकार संगठनों ने रिपोर्ट जारी कर इन घटनाओं को दर्ज किया। हज़ारों परिवार जंगल छोड़कर कैंपों और कस्बों में बसने को मजबूर हुए।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
जुलाई 2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सभी अर्धसैनिक सहयोगी बलों को तुरंत भंग किया जाए और नाबालिगों को हथियारबंद गतिविधियों से हटाया जाए।
यह फ़ैसला उन आदिवासी परिवारों के लिए राहत लेकर आया जिन्होंने वर्षों तक हिंसा और विस्थापन झेला था। लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर सलवा जुडूम जैसी नीतियों के असर लंबे समय तक बने रहे।
स्थायी असर
2005 से 2011 तक बस्तर ने भीषण हिंसा देखी।
- हज़ारों लोग विस्थापित हुए।
- कई बच्चे शिक्षा से वंचित रहे।
- गाँव की सामाजिक संरचना टूट गई।
- सैकड़ों निर्दोष लोग हिंसा की भेंट चढ़े।
आज भी बस्तर में सलवा जुडूम का ज़िक्र होते ही लोगों की आँखों में दर्द और डर झलक उठता है। यह केवल एक सुरक्षा नीति नहीं रही, बल्कि राज्य और समाज के बीच अविश्वास का प्रतीक बन गई।
निष्कर्ष
सलवा जुडूम भारतीय लोकतंत्र की उस विडंबना को दर्शाता है जहाँ शांति स्थापित करने के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया गया। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास और सुरक्षा की आड़ में आदिवासियों की ज़मीन और जीवन का बलिदान किया जा सकता है?
सलवा जुडूम केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि बस्तर के आदिवासी समाज के लिए पीड़ा और स्मृति का स्थायी घाव बन चुका है।
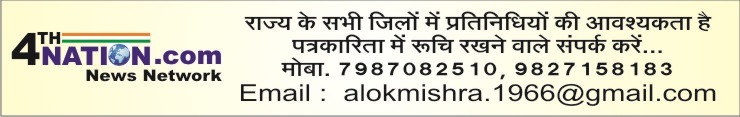
One thought on “सलवा जुडूम: बस्तर की जंग, राज्य की नीति और मानवाधिकारों का काला अध्याय”
Comments are closed.