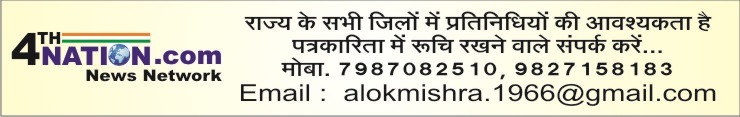नई दिल्ली, 26 जून 2025 — आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में घोषित आपातकाल (Emergency) को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। इस अवसर पर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आपातकाल की न केवल आलोचना हो रही है, बल्कि इसकी तुलना आज के दौर से भी की जा रही है, जिसे ‘अघोषित आपातकाल’ की संज्ञा दी जा रही है।
🗓 आपातकाल की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम
आपातकाल की पूर्वपीठिका 12 जून 1975 को तैयार हुई, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उसी समय बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन ज़ोर पकड़ चुका था, जिसकी कमान जयप्रकाश नारायण ने संभाली। छात्रों और युवाओं की ऊर्जा एक व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन में बदल गई थी, जो एकदलीय तानाशाही और कांग्रेस के केंद्रीकृत सत्ता मॉडल के विरुद्ध खड़ा था।
⚠️ सीपीएम सबसे पहले निशाने पर
आपातकाल की सबसे पहली झलक 1972 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी, जब CPM के खिलाफ पुलिस और गुंडों के गठजोड़ से चुनावों में धांधली की गई। अगले पाँच वर्षों में लगभग 1200 सीपीएम नेताओं की हत्या, हजारों कार्यकर्ताओं की बेदखली और आतंक का माहौल लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम था। केरल और त्रिपुरा में भी ऐसे ही प्रयास किए गए।
🔍 इमरजेंसी का प्रभाव: समाज और लोकतंत्र पर स्थायी आघात
25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के इन 21 महीनों में देश ने सेंसरशिप, गिरफ्तारी, यातना और भय का अभूतपूर्व दौर झेला। मगर इस आपातकाल ने केवल तत्कालीन भारत को नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति और समाज को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इससे सत्ता का केंद्रीकरण, संवैधानिक संस्थाओं की क्षति, और जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास जैसी स्थितियाँ बनीं, जो आज तक प्रभावी हैं।
सबक और चेतावनी
लेख में चेताया गया है कि इमरजेंसी से यदि कोई सबक नहीं लिया गया, तो इतिहास खुद को दुहराने को मजबूर होगा — पहले प्रहसन (comedy) के रूप में और फिर त्रासदी (tragedy) के रूप में। आज की संवैधानिक संकट और लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण को रोकने के लिए जरूरी है कि जनता सजग रहे और इतिहास से सीख ले।