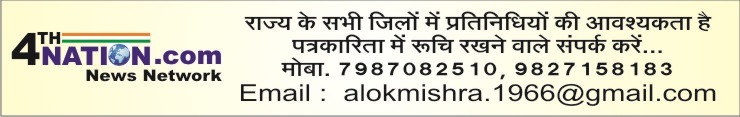नई दिल्ली, 24 जून 2025
भारत में अत्यधिक गरीबी मात्र 2.3% रह जाने और 17.1 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने के विश्व बैंक के हालिया दावे को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। भारत के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2022-23) के आधार पर आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-12 से लेकर अब तक अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह दावा जमीनी सच्चाई से बहुत दूर और आमजन के अनुभवों का अपमान है।
आर्थिक नीतियों ने बढ़ाया संकट
लेखक विमल कुमार की टिप्पणी के अनुसार, 2016 की नोटबंदी, 2017 में जीएसटी लागू करना, 2020 का कठोर लॉकडाउन, नए श्रम संहिता, और प्रस्तावित कृषि कानून — इन सभी सरकारी कदमों ने आम जनता की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। मनरेगा, सरकारी नौकरी, कृषि ऋण जैसी राहतकारी योजनाओं को या तो सीमित कर दिया गया या उनका असर कम कर दिया गया, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय तबकों पर संकट गहराया।
सांख्यिकी का फर्जीवाड़ा?
सरकार पर यह भी आरोप है कि उसने गरीबी के आंकड़े कम दिखाने के लिए घरेलू उपभोग सर्वेक्षण की पद्धति में बदलाव किए हैं। 2019 में सरकार ने सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने से इंकार कर दिया था, क्योंकि वे गरीबी में वृद्धि दर्शा रहे थे। बाद में, तीन बार सर्वेक्षण करके उपभोग की अधिक मात्रा दर्ज की गई जिससे खपत व्यय का अनुमान कृत्रिम रूप से बढ़ गया।
इसके अलावा, रिपोर्ट इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि 2011-12 और 2022-23 के सर्वेक्षण की पद्धतियाँ अलग थीं, जिससे दोनों के आंकड़ों की तुलना भ्रामक बन जाती है।
पीएलएफएस (PLFS) पर भी सवाल
पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें बकरी पालने वाली महिला या घर में बिना वेतन काम कर रही महिला को भी रोज़गार प्राप्त व्यक्ति माना गया है। ग्रामीण महिलाओं में इस तरह के ‘स्व-रोज़गार’ के आधार पर रोज़गार दर में वृद्धि का दावा किया गया है, जो हकीकत में बेहद कमजोर है।
सरकारी प्रचार बनाम जनता का अनुभव
कभी देश की शान रही भारत की सांख्यिकी प्रणाली को मोदी सरकार के दौर में प्रचार का माध्यम बना दिया गया है। गरीबों के वास्तविक जीवन संकटों को छुपाकर, झूठे आंकड़ों से सरकार यह दिखाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, जबकि मजदूर वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और ग्रामीण महिलाएं आज भी जीवन-यापन की बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं।
निष्कर्ष
विश्व बैंक की रिपोर्ट और सरकारी प्रचार से इतर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। आंकड़ों के इस भ्रम और सच्चाई के बीच की खाई को उजागर करना आवश्यक है ताकि जनता को ठोस तथ्यों के साथ संगठित किया जा सके और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनचेतना खड़ी की जा सके।