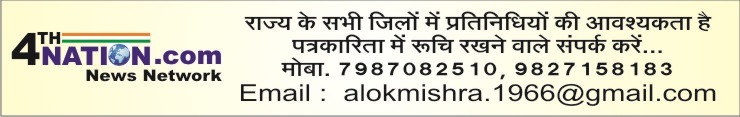दुर्ग, 04 अगस्त 2025| भारत का लोकतंत्र, जिसकी नींव संविधान, संस्थाएं और जनता के बीच संतुलन पर टिकी है, बीते एक दशक में गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। 2014 के बाद से जो राजनीतिक प्रवृत्तियाँ उभरी हैं, उन्होंने न केवल संविधान के मूलभूत ढांचे को चुनौती दी है, बल्कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया – को भी एक गहरी गिरावट में धकेला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया इस्तीफे और उससे जुड़ी घटनाएं इस गिरावट का जीवंत प्रमाण हैं।
संवैधानिक पतन की शुरुआत शीर्ष से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद संविधानिक मर्यादाओं का जैसा हनन शुरू हुआ, वैसा भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों को सरकार की कठपुतली बना देने की रणनीति ने संस्थाओं की आत्मा को जकड़ लिया। न्यायपालिका को दबाव में लाकर फैसले प्रभावित किए गए। मीडिया, जो लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता था, सत्ता का प्रचार माध्यम बन गया। और नौकरशाही – कभी तटस्थ सेवा संस्था – सत्ता की चाकरी में बदलती चली गई।
धनखड़: सत्ता के प्रति वफादारी की पराकाष्ठा
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पूरा कार्यकाल एक पार्टी विशेष की नीतियों और विचारधारा का अप्रत्यक्ष प्रवक्ता बनकर बीता। राज्यसभा में आरएसएस की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, उसे स्वयं आरएसएस के सबसे वरिष्ठ नेता भी सार्वजनिक रूप से कहने से बचते हैं। उनका यह बयान कि “आरएसएस की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है” भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए न केवल खतरनाक है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की सीधी अवहेलना भी है।
मगर फिर भी… वफादारी का ये इनाम?
इतनी कट्टर वफादारी के बावजूद जिस तरह से उन्हें धकियाकर बाहर किया गया, वह सत्ता के चरित्र को उजागर करता है – निष्ठा का इनाम नहीं, बल्कि जरूरत पूरी होने पर फेंक दिए जाने की प्रवृत्ति। बताया जा रहा है कि महज दो जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को संसदीय प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के चलते धनखड़ के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली गई। यह घटनाक्रम बताता है कि आज की सत्ता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कितनी असहजता से देखती है।
जजों के विवाद: न्यायपालिका में भी असंतुलन?
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के मामलों में न्यायिक निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उठे, वे स्वतः में चिंता का विषय हैं। मगर उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि इन मामलों पर संसदीय कार्यवाही रोकने के लिए संवैधानिक पदधारियों को सत्ता के इशारों पर हटाया जा रहा है। इससे साफ है कि “न्यायिक प्रक्रिया” का इस्तेमाल सिर्फ विरोधियों के लिए होता है – सत्ता के अपने लिए नहीं।
यह लोकतंत्र की बीमारी का लक्षण है
यह पूरी घटना सिर्फ एक व्यक्ति – धनखड़ – तक सीमित नहीं है। यह भारत के लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। संवैधानिक संस्थाओं का निजीकरण, विरोध की जगहों का संकुचित होना, और सत्ता से असहमति रखने वालों को सिस्टम से बाहर निकालने की परिपाटी – यह सब उस फासीवादी ढांचे की ओर बढ़ते कदम हैं, जिसकी आहट अब बहुत स्पष्ट हो चुकी है।
आगे क्या?
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लोकतंत्र की रक्षा से जोड़ते हुए सही दिशा में कदम उठाया है, मगर यह पर्याप्त नहीं है। इसे जन-जन तक पहुंचाना होगा। लोगों को यह समझाना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि संस्थाओं की स्वतंत्रता, असहमति का सम्मान और जवाबदेही का दायरा है।
अब समय आ गया है कि जनता इस सांड की तरह बेकाबू होती सत्ता को सींगों से पकड़े, वरना सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरा राष्ट्र बेआबरू होकर बाहर निकाला जाएगा।